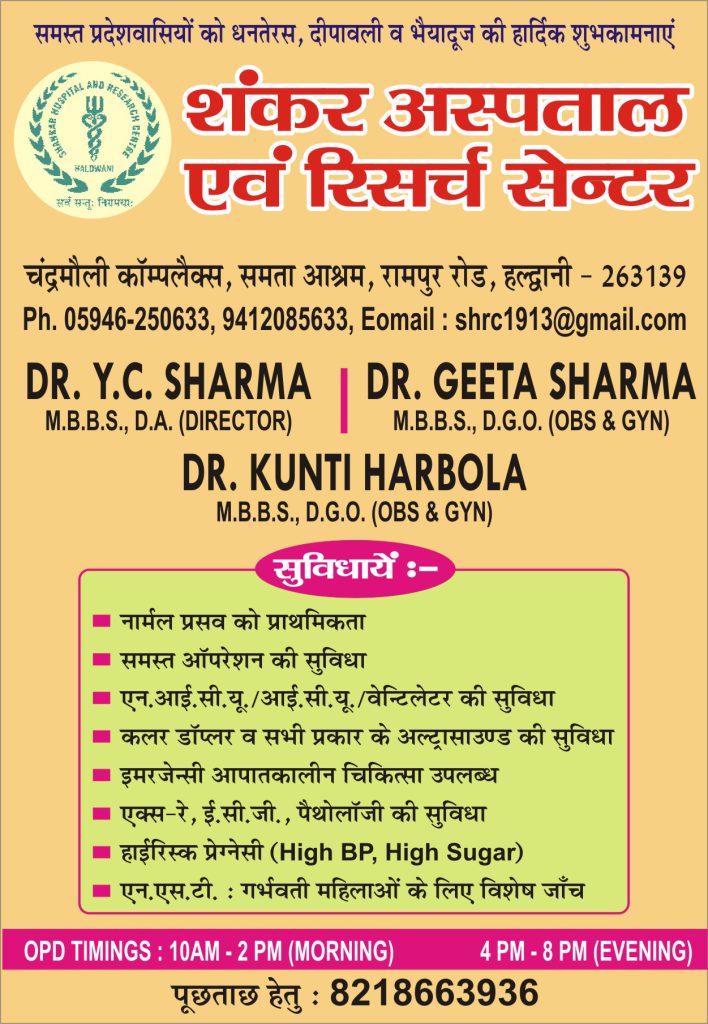राजेश सरकार
देहरादून: भारतीय राजनीति का इतिहास यह बताता है कि राजनीति का मुख्य उद्देश्य जनता की सेवा और उनके हितों की रक्षा करना है। समय के साथ राजनीति में ऐसे कई नेता हुए जिन्होंने अपनी निष्ठा और जनसेवा के माध्यम से राजनीति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लेकिन आज के दौर में राजनीति का अर्थ बदल चुका है। आज राजनीति में प्रवेश करने वाले अधिकांश नेता जनसेवा की बजाय अपने स्वहित को प्राथमिकता दे रहे हैं।
उत्तराखंड के 24 वर्षों के इतिहास से यह स्पष्ट होता है कि राज्य निर्माण के लिए पहाड़ की आवाज़ उठाने वाले नेताओं का मुख्य उद्देश्य जनहित से अधिक स्वहित रहा है। राज्य निर्माण के बाद, जबकि पहाड़ के विकास का सपना दिखाया गया, वास्तविकता यह है कि केवल नेताओं का ही विकास हुआ है। हल्द्वानी, देहरादून, और श्रीनगर जैसे स्थानों में पहाड़ी जनप्रतिनिधियों के भव्य बंगले इसकी मिसाल हैं।
अब एक बार फिर विधानसभा और लोकसभा सीटों के भौगोलिक परिसीमन की बात हो रही है। इसका तर्क यह दिया जा रहा है कि पहाड़ की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यदि परिसीमन किया जाए तो अधिक सीटें मिलेंगी, जिससे पहाड़ की समस्याओं को मंच मिलेगा और उनके विकास को गति मिलेगी। लेकिन इस तर्क का असली मकसद सिर्फ जनता को गुमराह करना है। सीटों की संख्या बढ़ाने से सबसे अधिक लाभ केवल नेताओं को ही होता है, जनता को नहीं।
पहाड़ का हाल तो आज भी वही है, युवा रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं। पहले तो कुछ साल बाद लौट आते थे, लेकिन अब वे कभी लौट कर नहीं आते। इससे पहाड़ वीरान और निस्तेज हो गया है। घरों में उग आई खरपतवार और सन्नाटा इसके गवाह हैं।
विधानसभा/लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने से विकास का दावा किया जाता है, लेकिन अभिभाजित उत्तर प्रदेश के दौरान पहाड़ में 19 विधानसभा सीटें थीं, जो राज्य गठन के बाद बढ़कर 70 हो गईं। इस बढ़ोतरी के बावजूद पहाड़ की स्थिति पहले से भी खराब हो गई। इसका मतलब यह है कि जनप्रतिनिधियों के लिए यह तो लाभकारी है, पर जनता के लिए नहीं।
जनप्रतिनिधियों के पहाड़ में न रहने के भी तर्क हैं। उनका कहना है कि पहाड़ की योजनाओं को पूरा करने के लिए जरूरी अधिकारी मुख्य रूप से मैदानी इलाकों में स्थित हैं। हालांकि, इस तर्क का असली प्रभाव यह है कि पहाड़ के दस जिलों के जनप्रतिनिधि हल्द्वानी, देहरादून, और हरिद्वार से ही पहाड़ की राजनीति चला रहे हैं।
नए जिलों के गठन, स्थाई राजधानी का छलावा
उत्तराखंड में नए जिलों के गठन और गैरसैंण को स्थाई राजधानी बनाने के मुद्दे ने राज्य की राजनीति में कई बार चर्चा का विषय बना है। हालांकि, इन मुद्दों पर कई बार घोषणाएं की गईं, लेकिन ये घोषणाएं धरातल पर उतरी नहीं और केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रह गईं।
राज्य गठन के बाद से नए जिलों की मांग लगातार उठती रही है। पहले मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर चार नए जिलों की घोषणा की थी, लेकिन ये योजनाएं अमल में नहीं आईं। इसके बाद, बीसी खंडूरी ने नए जिलों के गठन के लिए शासनादेश जारी किया, लेकिन बजट की कमी और अन्य प्रशासनिक अड़चनों ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। कांग्रेस सरकार के दौरान विजय बहुगुणा ने जिला पुनर्गठन आयोग का गठन किया, लेकिन इसके बावजूद कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। हरीश रावत ने तो नौ नए जिलों का वादा किया और इसके लिए 100 करोड़ रुपये का बजट भी रखा, लेकिन ये भी चुनावी वादा बनकर रह गया।
गैरसैंण को स्थाई राजधानी बनाने की मांग भी एक पुराना राजनीतिक मुद्दा है। 25 साल से अधिक समय बाद भी इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं हो पाया है। यह मुद्दा बार-बार राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बनता है, लेकिन इसके लिए वास्तविक प्रयासों की कमी रही है। हाल ही में परिसीमन प्रक्रिया के तहत मैदानी जिलों में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ने और पर्वतीय जिलों में घटने की संभावना है। इससे राजनीतिक दलों की प्राथमिकताएं बदल सकती हैं। इस बदलाव के बाद, गैरसैंण को स्थाई राजधानी बनाने की संभावना एक बार फिर से उठ सकती है, लेकिन यह तभी संभव होगा जब राजनीतिक इच्छाशक्ति और पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता हो।
इन सभी पहलुओं से यह स्पष्ट होता है कि नए जिलों के गठन और गैरसैंण को राजधानी बनाने के वादों ने राज्य की राजनीति में केवल छलावा किया है। राजनीतिक दलों की घोषणाओं में वास्तविकता की कमी और संसाधनों की बाधाएं इन परियोजनाओं के पूरा होने की राह में मुख्य अड़चनें रही हैं।