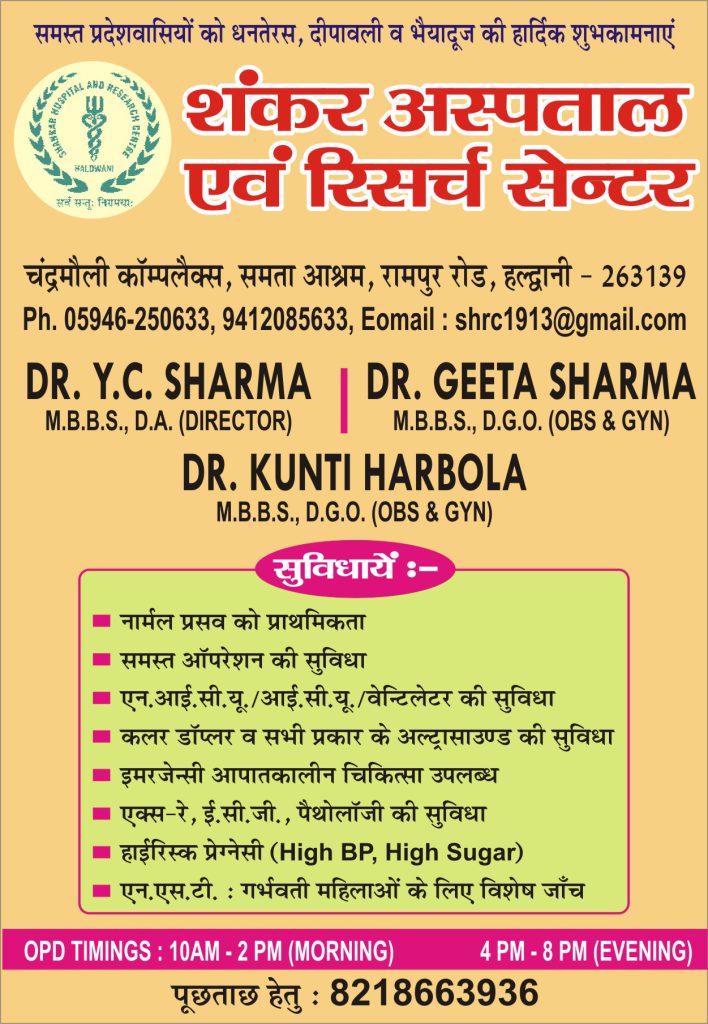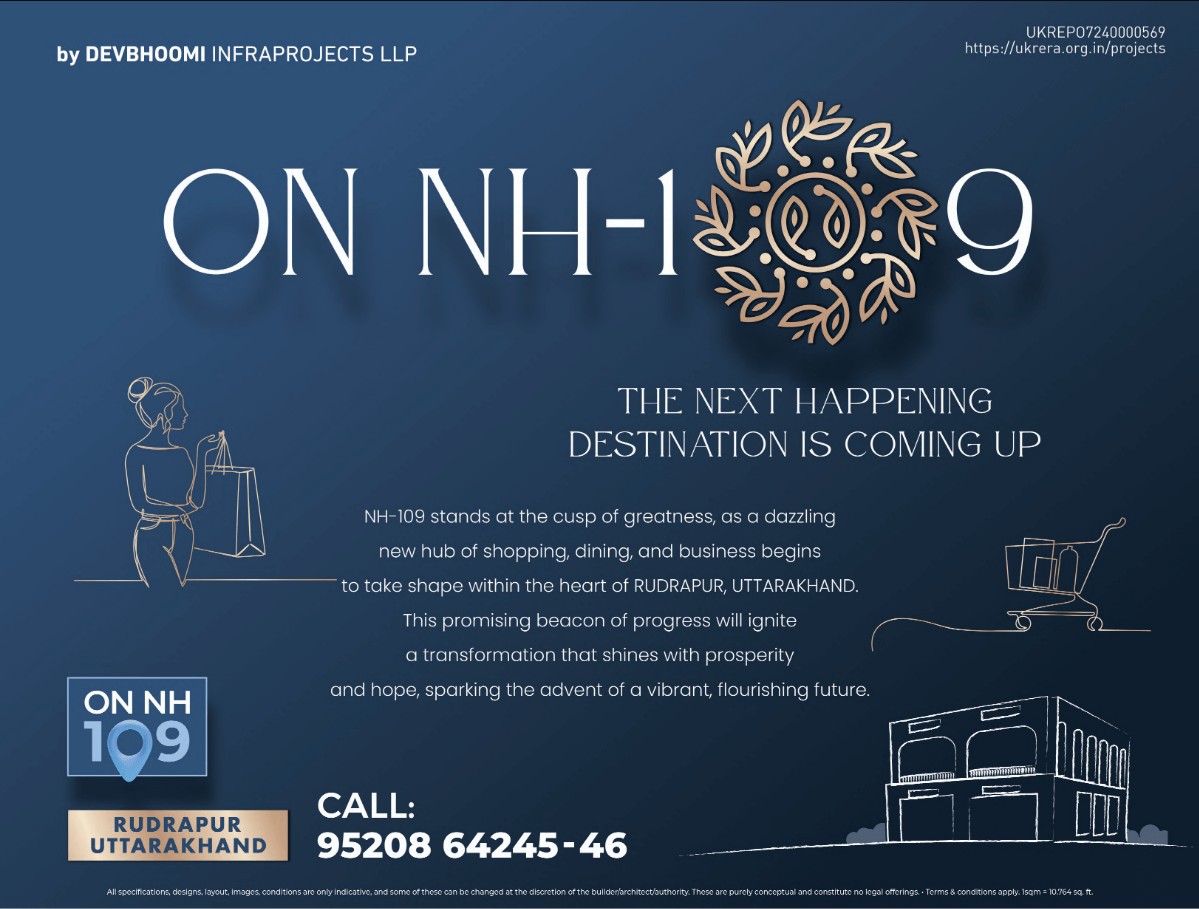

विजय बहुगुणा और सौरभ बहुगुणा: बुघाणी गांव से सितारगंज तक का सफ़र, त्रिवेंद्र सिंह रावत: पौड़ी के हैं, लेकिन राजनीति देहरादून और हरिद्वार में
देहरादून: उत्तराखंड के पहाड़ों का दर्द हर चुनाव में सुना जाता है पलायन का दर्द, खाली होते गांवों का दर्द, बंद स्कूलों और वीरान खेतों का दर्द। लेकिन जब नजर घुमाइए तो वही नेता जो मंचों से ‘पलायन रोकने’ की कसम खाते हैं, खुद मैदानों की राजनीति में टिके हैं, वहीं मकान बना चुके हैं और वहीं से जनता की सेवा करने की कसमें खा रहे हैं। राजनीतिक पलायन उत्तराखंड का शायद सबसे स्थायी राजनीतिक ट्रेंड बन चुका है।
हरीश रावत, जो कभी पहाड़ के बेटे कहलाए, आज हरिद्वार की मैदानी राजनीति में अपनी ज़मीन तलाशते रहे हैं। उनके भाषणों में अल्मोड़ा की मिट्टी की खुशबू होती है, लेकिन चुनाव की बयार हरिद्वार की गलियों से बहती है। कुमाऊं से गढ़वाल, हर मैदान में किस्मत आज़माने का पूरा प्रयास उन्होंने किया है।
त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिनके नाम के साथ ‘रावत’ जुड़ा है जो पहाड़ की पहचान है उन्होंने भी डोईवाला और फिर हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में अपना राजनीतिक ठिकाना ढूंढा। कहते हैं पहाड़ों से प्रेम है, लेकिन टिकट की राजनीति में प्रेम अक्सर देहरादून की सड़कों पर उतर आता है।
विजय बहुगुणा का परिवार तो जैसे ‘पलायन का राजनीतिक प्रतीक’ बन गया। पौड़ी जिले का मूल निवासी परिवार, लेकिन राजनीति का केंद्र सितारगंज। पिता इलाहाबाद में शिक्षित, बेटे की राजनीति भी मैदान में। पहाड़ से रिश्ते पोस्टर और भाषणों में ज़रूर बच गए हैं, पर ज़मीन की राजनीति पूरी तरह मैदानों में शिफ्ट हो चुकी है।
हरक सिंह रावत भी इस पलायन की कहानी के एक और किरदार हैं। कभी कोटद्वार से, कभी रुद्रप्रयाग से, और इच्छा रही तो हरिद्वार से। पहाड़ों के लिए भाषण अलग, टिकट की राजनीति के लिए भूगोल अलग।
जब युवाओं से उम्मीद थी कि वे ‘नई सोच’ लेकर आएंगे, तब भी वही पुरानी राह चली। अनुपमा रावत, हरीश रावत की बेटी ने हरिद्वार ग्रामीण सीट चुनी। भाजपा के खजानदास ने टिहरी छोड़कर देहरादून का रुख किया। सफाई यह कि सीट आरक्षित नहीं थी लेकिन यह सफाई सुनकर पहाड़ का कोई खाली गांव भी मुस्कुरा उठेगा।
दरअसल, राजनीतिक पलायन के पीछे सिर्फ़ सुविधा है। पर्वतीय इलाकों में एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंचना आसान नहीं। सड़कें टूटी हैं, इलाक़े दूर-दूर फैले हैं। प्रचार में वक्त भी ज़्यादा लगता है, खर्चा भी। मैदानों में सबकुछ आसान है सड़कें, मतदाता और सत्ता के गलियारे।
परिसीमन के बाद पहाड़ी जिलों की सीटें घटीं, मैदानों की बढ़ीं। पहाड़ के वोटर अब मैदानों में भी हैं। इसलिए नेता भी उसी दिशा में बह निकले जैसे नदियां मैदान की ओर उतरती हैं। फर्क सिर्फ़ इतना है कि नदियां जीवन देती हैं, और यह राजनीति बस वादे देती है।
विडंबना यह है कि पलायन पर सबसे ज़्यादा चिंता जताने वाली पार्टियों के दफ्तर भी देहरादून, हरिद्वार और हल्द्वानी में हैं। यहां तक कि ‘उत्तराखंड क्रांति दल’ जो पहाड़ की राजनीति का प्रतीक कहा जाता है उसका मुख्यालय भी देहरादून में है। रजत जयंती वर्ष में उत्तराखंड का सवाल वही पुराना है पहाड़ खाली क्यों हो रहे हैं? लेकिन अब यह सवाल जनता से पहले नेताओं से पूछा जाना चाहिए आप पहाड़ से भागे क्यों? क्यों हर बार मंचों से कहा जाता है हम पलायन रोकेंगे, और अगले ही दिन पहाड़ों की सीट छोड़कर मैदान की ओर कूच कर लिया जाता है?
जब नेता, व्यापारी, अफसर सब मैदान की ओर उतर आए हैं, तो पहाड़ में रह कौन गया है? किसके लिए बने वो स्कूल जो बंद पड़े हैं, वो सड़कें जिनसे अब कोई नहीं गुजरता? शायद अब उत्तराखंड में पलायन को समस्या नहीं, बल्कि राजनीतिक रणनीति कहना ज़्यादा सही होगा। क्योंकि यहां पलायन केवल रोज़गार या जीवन का नहीं चरित्र का भी है।
क्योंकि जब नेता पलायन को अपने भाषणों में दर्द बनाते हैं, तो वह दर्द दरअसल उनके अपने कदमों के नीचे दबा हुआ होता है।